
मई 1822 की बात है। नायरों ने शनार जाति की महिलाओं पर हमला करके उनके कपड़े फाड़ दिये। ऐसा क्यों किया ? क्योंकि जाति आधारित ऊँच-नीच से बनी सामाजिक व्यवस्था में शरीर के उपरी हिस्से पर कपड़े धारण करने का अधिकार केवल प्रभुत्वशाली जातियों के पास ही था। दलित जातियों ने जब-जब पहनावे से जुड़ी आचार सहिंता को चुनौती दी तब-तब हिंसक सामाजिक प्रतिक्रियाएँ आई। त्रावणकोर रियासत में जहाँ शनार जाति की महिलाएँ कपड़े पहनकर अपना मनपसंद जीवन जीने की कोशिश कर रही थी तो वहीं नायर जाति के लोग इसे अपनी शान के खिलाफ समझ रहे थे। संघर्ष बना रहा। सन् 1829 में सरकार ने एक घोषणा की जिसमें यह हिदायत दी गई कि शनार जाति की महिलाएँ शरीर के उपरी हिस्से को ढकने से बचे। सन् 1855 तक आते-आते त्रावणकोर रियासत में दास प्रथा ख़त्म हो गई थी। शनार महिलाएँ पहले की तुलना में अधिक मुखर होकर प्रभुत्वशाली जाति का सामना कर रही थीं। कुंठित नायर जाति के लोगों ने अक्टूबर 1859 में, बाज़ार के बीचों बीच शनार जाति की महिलाओं के कपडे फाड़कर अपने भोंडेपन का प्रदर्शन किया। यानी भारत में पहनावा जाति व्यवस्था के साथ भी नथा-गूंथा है। पहनावे को लेकर समाज जो कानून तय करता है उसे समुदाय धरातल पर लागू करता है।
समाज नाम की इस काल्पनिक संस्था ने 'कौन क्या पहनेगा' मुद्दे पर विभिन्न तबकों के लिए कुछ न कुछ नियम बनाएँ हुए हैं। कपड़ों के जरिये समाज ने सौम्यता और सुन्दरता, शर्म व मर्यादा की परिभाषाएँ गढ़ी हैं। जब समाज में पितृसत्ता हावी होती हैं तब उस समाज के अधिकांश कानून-कायदे महिलाओं को अधीन रखने के विचार से प्रेरित होते हैं। यह भी सही है कि जैसे-जैसे समाज के मूल्यों में बदलाव आता है वैसे-वैसे पहनावे में बदलाव आता है; सुन्दरता और मर्यादा की परिभाषा में बदलाव आता है।
आज का लेख, महिलाओं के कपड़ों का निर्धारण करने में समाज, समुदाय और परिवार की भूमिका पर केन्द्रित है। कैसे समाज ने महिलाओं के कपड़ों का निर्धारण कर पितृसत्ता और भारत के परिपेक्ष में जाति आधारित ऊँच-नीच को मजबूती दी ? इसी सवाल का जवाब है आज का लेख।
प्राचीन भारत के शुरुआत में शरीर के उपरी हिस्सों पर कपड़े नहीं पहने जाते थे। उस समय के मंदिरों को देखें तो उनमें बनी हुई मूर्तियों में देवियों के ऊपरी हिस्से पर कपड़े नहीं हैं। क्योंकि महिलाओं के स्तनों को नहीं ढकना असभ्य की श्रेणी में नहीं आता था। धीरे-धीरे वस्त्र पहने जाने लगे। एकःवस्त्रा, द्वि-वस्त्रा और त्रि-वस्त्रा का पहनावा प्रचलन में आया। इसी का विकसित रूप साड़ी बना।
जैसे-जैसे हिन्दू धर्म दुसरे धर्मों के सम्पर्क में आता गया वैसे-वैसे शरीर के साथ 'शर्म' की अवधारणा मजबूत होती गई। शरीर को शैतान और पापी का प्रतीक समझा जाने लगा। शरीर के खास हिस्से को दिखाना शर्मनाक माना जाने लगा। शरीर को ढकना शुरू किया गया। यहीं से साड़ी के साथ ही घूँघट का रिवाज शुरू हुआ। तथाकथित ऊँची जातियों और कुलीन परिवारों के लिए यह कानून और कड़े होते गए। महिलाओं को परदे में रखा जाने लगा। उनका पुरुषों के साथ मेल-झोल कम हो गया।
संभवतः किसी भी देवी-देवता को इस बात से फ़र्क नहीं ही पड़ता होगा कि उसका भक्त क्या पहन रहा है और क्या ओढ़ रहा है। लेकिन, समाज के कुछ ठेकेदारों ने धर्म का सहारा लेकर आचार संहिताएँ बनाना शुरू कर दिया। और कपड़ों से जुड़े नियमों को धर्म से जोड़ दिया।
चूँकि पहनावे से जुड़े नियमों का निर्माण समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग कर रहा था। ऐसे में इन नियमों का सबसे पहले सामना प्रभुत्वशाली वर्ग की महिलाओं को करना पड़ा। इन नियमों के जरिये प्रभुत्वशाली वर्ग, अपने वर्ग की महिलाओं को सभ्य रूप देना चाहता था। अपने वर्ग की महिलाओं को तथाकथित निम्न जाति की महिलाओं से अलग दिखाना चाहता था। आपने त्रावणकोर राज्य की उस घटना से अंदाजा लगाया होगा।
मध्यकाल को सामन्ती युग भी कहा जाता है। इस दौर तक आते-आते पितृसत्ता और अधिक मजबूत हो गई थी। जैसे-जैसे समाज में पितृसत्ता मजबूत होती गई वैसे-वैसे महिलाओं के ऊपर बंदिशे बढ़ती गई। यही हाल पश्चिम देशों का था। आपने सम्प्चुअरी कानूनों के बारे में सुना ही होगा। इन कानूनों का मकसद था समाज के खास तबकों (महिला और दासों) को नियंत्रण में रखना। कॉर्सेट जैसे पहनावे का प्रचलन इस बात की गवाही देता है।
आगे जाकर रैशनल ड्रेस रिफार्म आन्दोलन ने पहनावे के ऊपर बनी हुई संहिताओं को चुनौती दी। जिसमें अमेलिया ब्लूमर का योगदान प्रमुख है।
औपनिवेशिक भारत में पहनावे का मुद्दा
अठाहरवीं सदी के बाद दुनिया के अधिकांश हिस्से यूरोपीय देशों के उपनिवेश बन गए थे। वहाँ जनतांत्रिक आदर्शों का प्रसार हुआ। चूँकि जनतांत्रिक विचारों में वेशभूषा से जुड़े ख़यालात भी शामिल होते हैं। ऐसे में आधुनिक दुनिया के उदय के इतिहास में पहनावे में आएँ नाटकीय बदलावों का इतिहास भी शामिल है।
इस दौर में भारत में क्या हो रहा था ? भारत में दो तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही थीं। पहली प्रतिक्रिया प्रभुत्वशाली वर्ग की महिलाएँ की तरफ से आ रही थी और दूसरी, तथाकथित निम्न जाति की महिलाओं की तरफ से।
औपनिवेशिक शासनकाल में गोरे अधिकारियों के साथ पश्चिमी पहनावा भी भारत आया। मिशनरी के लोगों ने जब काम करना शुरू किया तब पहनावा और अधिक प्रचारित हुआ। कई मर्दों ने इसे अपना लिया। इस पर ज्यादा हो-हल्ला नहीं हुआ। लेकिन, जैसे ही प्रभुत्वशाली वर्ग की महिलाओं ने पश्चिमी परिधानों को अपनाने की कोशिश की तो उसका प्रतिरोध शुरू हो गया।
प्रभुत्वशाली वर्ग के मर्दों ने अपने वर्ग की महिलाओं के लिए खास तरह की वस्त्र संहिताएँ तैयार की थी। जिसमें महिला की छवि एक दब्बू और निर्बल-अबला महिला की बनती थी। जो कि घूँघट में रहती है। ये महिलाएँ इससे आज़ादी चाहती थीं। और पश्चिमी परिधानों को मुक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा था। यानी विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि महिलाएँ इसके जरिये आज़ाद अनुभव कर रही थीं। आज भी जब पश्चिमी परिधानों का विरोध किया जाता है तब ठेकेदारों द्वारा संस्कृति और परम्परा की आड़ ली जाती है। जबकि इसके पीछे की असली वजह है- आज़ादी।
हमने लेख की शुरुआत शनार (नाडर) जाति की महिलाओं के साथ किये गए अत्याचार से की थी। उन महिलाओं की मांग क्या थीं ? वो अपने शरीर के उपरी हिस्से को ढकना चाहती थीं। और यह बात नायर जाति के लोगों को हज्म नहीं हो रही थी। क्योंकि प्रभुत्वशाली वर्ग ने परिधानों को धारण करना सभ्य होने की एक निशानी माना था। ऐसे में उन्हें यह डर था कि कहीं तथाकथित निम्न जाति के लोग कपड़े पहनकर सभ्य-असभ्य नाम की इस खोखली दुनिया का भांडा फोड़ न दे। वहीं दमित जाति के लोग वस्त्र पहनकर स्वाभिमान वाला जीवन जीना चाहते थे।
वहीं देश के कई और हिस्सों में दलित वर्ग की महिलाएँ प्रभुत्वशाली वर्ग की महिलाओं की तरह अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी। इस पर प्रभुत्वशाली वर्ग के लोगों को ऐतराज था।
आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने पोशाक को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया था। अधिकांश लोग खादी के वस्त्रों को पहनने लगे थे। हालाँकि, खादी के वस्त्र तुलनात्मक रूप से महंगे आते थे ऐसे में कई दमित जाति के लोगों के लिए खरीदना मुश्किल होता था।
आज़ाद हिंदुस्तान में
आज़ाद हिंदुस्तान में दोनों चुनौतियाँ बनी हुई थीं या यूँ कहे बनी हुई हैं। प्रभुत्वशाली वर्ग की महिलाएँ पश्चिमी परिधानों को अपनाने की कोशिश कर रही हैं।कई परिवार इसे स्वीकार कर देते हैं। तो कई परिवारों में अभी भी पितृसत्ता हावी है। हरियाणा में खाप पंचायतों के फैसले इस बात को पुख्ता करते हैं। अगर वाकई पश्चिमी संस्कृति से दिक्कत है तब मर्दों के मामले में यही पैमाना क्यों नहीं अपनाया जाता है। असली डर किस बात का है ?
दलित वर्ग की महिलाएँ जब अपनी पसंद का कपडा पहनती हैं तब प्रभुत्वशाली जाति के लोग विरोध करते हैं। और इस विरोध को दलित जाति के पुरुष मजबूती देते हैं। दलित मर्दों को महिलाओं की ऐसी पसंद से दिक्कत क्यों है ? कहीं न कहीं दलित पुरुष भी उसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का खेवनहार है।
परिवार और समुदाय, समाज का हिस्सा होते हैं। समाज जिन कानून-कायदों को तैयार करता है समुदाय उसकी निगरानी करता है और परिवार उसे लागू करता है।
क्या पहनना है, क्या ओढना है यह व्यक्ति की निजी पसंद-नापसंद है। लेकिन, समाज के शक्तिशाली वर्ग (मर्द और तथाकथित उच्च जाति) ने हमेशा ही अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इसे एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया है। कई बार इसके लिए धर्म की आड़ ली, तो कई बार संस्कृति और राष्ट्रवाद की। ऐसे में पहनावे के इतिहास समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। जैसे-जैसे समाज में बदलाव आएगा वैसे-वैसे सामाजिक मूल्यों में बदलाव आएगा। ज़नानापन और खूबसूरती के पैमानों में बदलाव आएंगा। आज हिंदुस्तान सामाजिक मूल्यों में बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

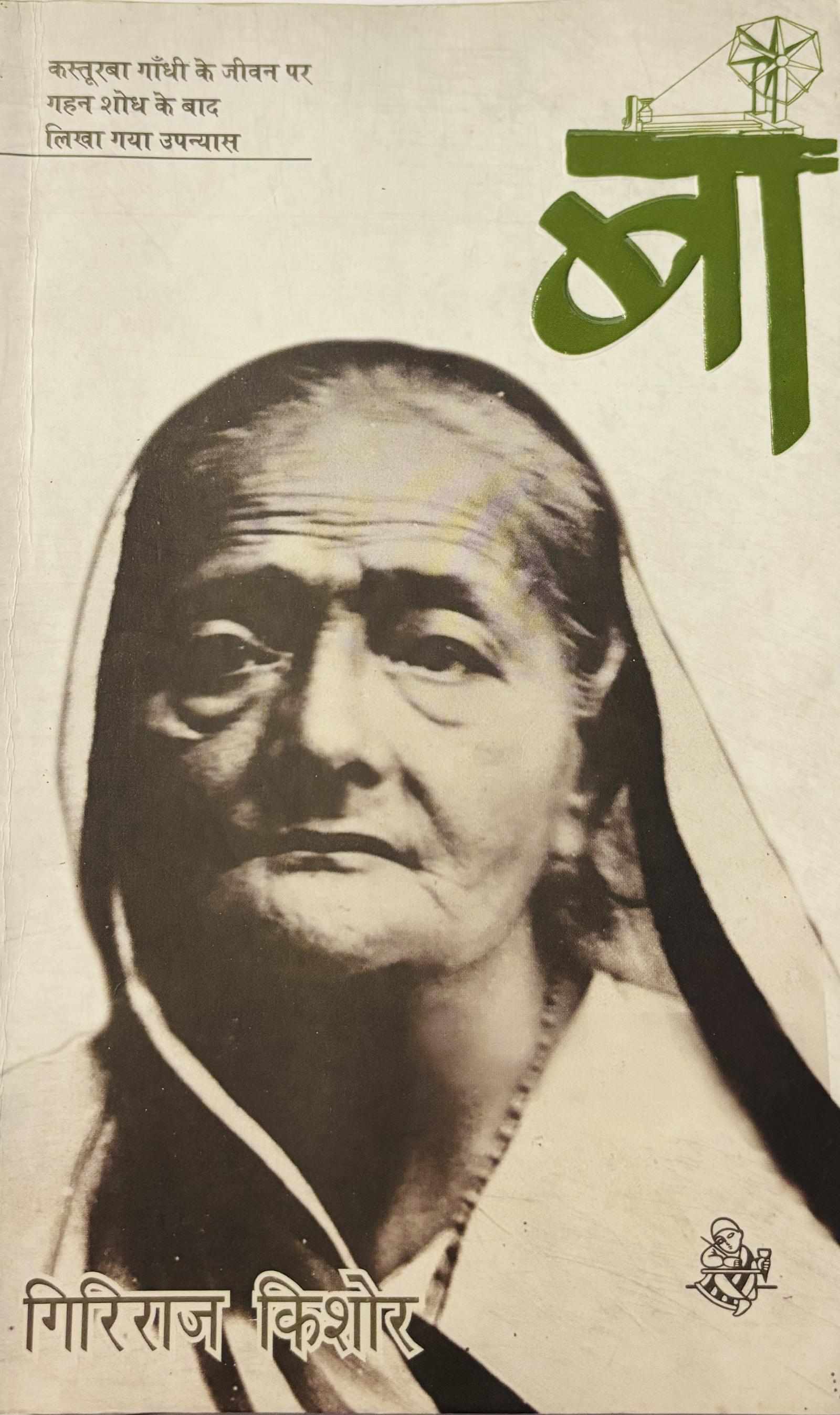







Write a comment ...